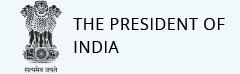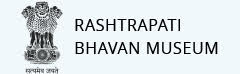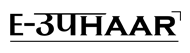उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों को ‘संसद और नीति निर्माण’ विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति, श्री प्रणब मुखर्जी का नव-वर्ष का संबोधन
राष्ट्रपति भवन : 19.01.2015
डाउनलोड : भाषण ![]() (हिन्दी, 508.18 किलोबाइट)
(हिन्दी, 508.18 किलोबाइट)
 कुलपतिगण,
कुलपतिगण,
निदेशकगण,
उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के अध्यक्षगण,
संकाय सदस्यगण, और
प्यारे विद्यार्थियो,
1. सर्वप्रथम मैं आपको और आपके परिवारों को एक अत्यंत खुशहाल और समृद्ध नव-वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। वर्ष के आरंभ में ही आपके सामने अपने कुछ विचारों को व्यक्त करने का अवसर प्राप्त करके मुझे प्रसन्नता हुई है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इतनी बड़ी संख्या में, मेरे लिए आप तक पहुंचना संभव बनाने के लिए,मैं राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क टीम, विशेषकर प्रो. एस.वी. राघवन तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान टीम की सराहना और आभार व्यक्त करता हूं। गत वर्ष यह निर्णय लिया गया था कि मैं आपको दो बार—एक बार जनवरी में नव-वर्ष के प्रारंभ में तथा दूसरी बार अगस्त में नए शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में संबोधित करूंगा।
मित्रो,
2. 2014 का वर्ष भारत की राजव्यवस्था के लिए एक महत्त्वपूर्ण वर्ष था। तीन दशकों के बाद,भारतीय मतदाताओं ने एक स्थिर सरकार बनाने के लिए एक अकेले दल को बहुमत देने का निर्णय लिया।16वीं लोकसभा के चुनावों के परिणामों से राजनीतिक स्थिरता आई है तथा चुनी गई सरकार को नीतियों के निर्माण में तथा उन नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कानून बनाने में अपने बहुमत का प्रयोग करके अपनी जनता से अपने वायदों को पूरा करने का जनादेश प्राप्त हुआ है।
संस्थानों के विशिष्ट अध्यक्षगण, संकाय सदस्यगण और प्यारे विद्यार्थियो,
3. एक लोकतांत्रिक राजव्यवस्था में,राष्ट्र का निर्माण और सशक्तीकरण सरकार के सभी प्रमुख अंगों का सामूहिक दायित्व है। संसदीय लोकतंत्र में सभी तीनों अंग-कार्यपालिका,विधायिका (संसद) तथा न्यायपालिका सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यकारी अंग हैं। तीनों संविधान से शक्ति प्राप्त करते हैं जिसमें नीति निर्माण,विधायन, नीतियों और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन तथा जब भी आवश्यकता हो,न्यायपालिका द्वारा कानून की व्याख्या करने की उनकी भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है।
4. आज, मैंने, ‘संसद और नीति निर्माण’विषय अथवा सामान्य शब्दों में ‘विधि और नीति के बीच संबंध’विषय पर बोलने का निर्णय किया है। आप मानेंगे कि इस तरह मुद्दे पर चर्चा करने से संसद तथा कार्यपालिका के साथ-साथ न्यायपालिका भी देश की विकास प्रक्रिया को तेज करने में एक महत्त्वपूर्ण भागीदार बन जाती है। सभी तीनों अंगों से बिना एक दूसरे का अतिक्रमण किए संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।
मित्रो,
5. किसी भी लोकतंत्र में संसद के तीन अत्यावश्यक कार्य होते हैं। प्रतिनिधित्व,कानून निर्माण तथा निगरानी। यद्यपि नीति निर्माण और विधायन की शुरुआत मुख्यतया कार्यपालिका का कार्य है,परंतु विधान का निर्माण अथवा इसकी अस्वीकृति विधायिका का कार्य क्षेत्र है। कानूनों की व्याख्या न्यायपालिका का कार्य क्षेत्र है।
6. संसद जनता की इच्छा और अकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। यह ऐसा मंच है जहां परिचर्चा तथा विचार-विमर्श के द्वारा इस‘इच्छा’और ‘आकांक्षाओं’की प्राथमिकता तय करके उसे कानूनों, नीतियों और ठोस कार्य योजनाओं में बदलना होता है। जब ऐसा नहीं होता तब लोकतंत्र के संचालन में किसी महत्त्वपूर्ण तत्त्व में बाधा आती है तथा उसका नुकसान जनता को होता है।
मित्रो,
7. कानून का अर्थ, समाज में लोगों और समुदायों के बीच सामाजिक रिश्तों के संचालन के लिए स्थापित संहिताबद्ध अथवा पारंपरिक व्यवहार में निहित सिद्धांतों और नियमों से है। इससे दो महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हैं। इससे सामाजिक मूल्यों को आकार मिलता है और इनके प्राप्ति की आकांक्षा के आयामों को मजबूती मिलती है। यह वांछित सामाजिक लक्ष्यों की दिशा में मानव व्यवहार का मार्गदर्शन करने में मदद करता है। इस प्रकार,परिभाषा के अनुसार,विधि सार्वजनिक नीति के संचालन का नियामक आधार तथा ढांचा प्रदान करती है
8. हमारे संसदीय लोकतंत्र में कानून का निर्माण अथवा विधायन संसद तथा विधान सभाओं का एक एकांतिक कार्य है। विधेयक पारित करने का कार्य कानून निर्माण का आसान हिस्सा होता है (बहुमत न होने पर यह कार्य इतना सरल नहीं होता)। इसका कठिन हिस्सा इस कानून के लिए विभिन्न समूहों के हितों के बीच तालमेल बिठाने के लिए बातचीत करना होता है। कोई विधायिका तभी प्रभावी होती है जब वह स्टेकधारकों के बीच मतभेदों का समाधान करने में सफल हो तथा कानून के निर्माण तथा उसको लागू किए जाने के लिए एकमत कायम करने में सफल हो। जब संसद कानून निर्माण की अपनी भूमिका का पूरा करने में असफल रहती है अथवा बिना चर्चा किए कानून बनाती है तो यह जनता द्वारा उसमें व्यक्त किए गए विश्वास को तोड़ती है। यह न तो लोकतंत्र के लिए अच्छा है और न ही उन कानूनों के द्वारा शुरू की गई नीतियों के लिए अच्छा है।
संस्थानों के विशिष्ट अध्यक्षगण, संकाय सदस्यगण तथा प्यारे विद्यार्थियो,
9. नीति का अर्थ किसी निश्चित स्थिति में अपेक्षित परिणाम शीघ्र प्राप्त करने और सुगम बनाने के लिए की गई कार्रवाई के एक निर्धारित प्रक्रिया से है। इसका स्वरूप नियामक है। ये नियम विधि तथा समाज में व्याप्त सामाजिक प्रथाओं से,अथवा उन अंतरराष्ट्रीय समझौतों से निर्मित होते हैं जिसका कोई राष्ट्र एक पक्षकार होता है। नीतियों को व्यापक राष्ट्रीय हित में समाज के विभिन्न भागीदारों की चिंताओं पर आवश्यक रूप से ध्यान देना होगा।
मित्रो,
10. भारत के संदर्भ में नीति निर्माण का मार्गदर्शन संविधान द्वारा होता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत,सभी कार्यकारी और विधायी कार्रवाई का आधार प्रदान करने के लिए सकारात्मक अनुदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सिद्धांत गैर-न्यायाधीन हैं,परंतु देश के शासन के मौलिक तत्त्व हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के1973 के ऐतिहासिक निर्णय में, उच्चतम न्यायालय का मत था कि नीतिनिर्देशक सिद्धांत तथा मौलिक अधिकार दोनों समान रूप से मौलिक हैं,भले ही नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालयों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं। विगत दशक के दौरान,विधिक गारंटी के जरिए लोगों को सूचना का अधिकार, ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित रोजगार सुरक्षा, शिक्षा और भोजन के अधिकार के हक प्रदान किए गए हैं। प्रत्येक वैधानिक हस्तक्षेप से नीति में हमारे संविधान में निर्धारित उद्देश्यों की दिशा में बदलाव आया है तथा यह मानवीय कल्याण की ओर बढ़ी है।
मित्रो,
11. नीतियों के निर्माण में सहायता के उपरांत संसद यह भी सुनिश्चित करती है कि जिन नीतियों और कार्यक्रमों को तय करने में उसने सहयोग किया है वह परिकल्पना के अनुसार कार्यान्वित हों। यह इस बात पर भी नजर रखती है कि इन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कार्यपालिका द्वारा कानून सम्मत,कारगर ढंग से तथा उसी उद्देश्य से हो जिसके लिए उन्हें बनाया गया था। संसद की यह निगरानी अन्य दो कार्यों में भी आती है। संसद के पास धन और वित्त पर पूर्ण नियंत्रण की एकांतिक शक्ति होती है। प्रत्येक कर तथा प्राप्ति तथा भारत की समेकित निधि में तथा उसमें से कोई भी व्यय लोक सभा अथवा विधान सभा के अनुमोदन के उपरांत ही हो सकता है। कार्यपालिका पर संसद की एक दूसरी महत्त्वपूर्ण निगरानी शक्ति यह है कि सर्वोच्च कार्यपालक प्राधिकारी अर्थात प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल तभी तक कार्य कर सकते हैं जब तक उन्हें जनता द्वारा चुने गए सदन का विश्वास हासिल होता है तथा उन्हें अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सदन के साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है। हमारे संविधान के अनुसार,कुछ आपवादिक परिस्थितियों में, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सदन के त्रिशंकु होने तथा इसके कामकाज के अनियमित और असमंजित होने पर लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। इसलिए,कार्यपालिका के ये दो अत्यंत महत्त्वपूर्ण कामकाज जनता द्वारा निर्वाचित सदन के संपूर्ण नियंत्रण के अधीन हैं।
12. नीतियों की व्याख्या करने,उसके कार्यान्वयन तथा उस पर नजर रखने में संसद की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती है। इसलिए यह संसद सदस्यों की जिम्मेदारी है कि सदन में किए जा रहे सभी कामकाज पर चर्चा करें तथा समुचित छानबीन करें। दुर्भाग्यवश, संसद में सदस्यों द्वारा लगाए जा रहे समय में धीरे-धीरे कमी आती जा रही है। जहां पहली तीन लोक सभाओं की क्रमश:677, 581 तथा 578बैठकें हुई थीं वहीं13वीं, 14वीं तथा 15वीं लोक सभाओं की क्रमश: केवल356, 332 तथा 357 बैठकें हुई। हम सभी को यह उम्मीद करनी चाहिए कि16वीं लोक सभा में यह रुझान बदलेगा।
मित्रो,
13. संसदीय हस्तक्षेप के एक साधन के रूप में व्यवधान करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। यद्यपि असहमति एक मान्य संसदीय अभिव्यक्ति है परतु व्यवधानों से समय और संसाधनों की बर्बादी होती है तथा नीति निर्माण ठप हो जाता है। संसदीय लोकतंत्र का मूल सिद्धांत यह है कि बहुमत को शासन करने के लिए अधिदेश प्राप्त है तथा विपक्ष को विरोध करने,उजागर करने तथा पर्याप्त संख्या होने पर अपदस्थ करने का अधिकार हासिल है। परंतु किसी भी हालत में कार्यवाही में व्यवधान नहीं होना चाहिए। शोरशराबा करने वाले अल्पमत को धैर्यवान बहुमत की आवाज को दबाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
प्यारे विद्यार्थियो,
14. कुछ तात्कालिकताओं के समाधान के लिए तथा बाध्यकारी परिस्थितियों में,संविधान के निर्माताओं ने यह जरूरी समझा था कि वह कार्यपालिका को उस समय के लिए अध्यादेशों के प्रख्यापन के रूप में कानून निर्माण की सीमित शक्ति प्रदान करे जब विधायिका का सत्र न चल रहा हो और परिस्थितियां तत्काल कानून निर्माण के लिए औचित्यपूर्ण हों। संविधान निर्माताओं ने यह भी जरूरी समझा था कि वह संविधान में इस तरह के अध्यादेशों की एक निश्चित समय सीमा के अंदर विधायिका द्वारा प्रतिस्थापन की व्यवस्था द्वारा इस असाधारण कानूनी शक्ति पर कुछ प्रतिबंध लगाए। अनुच्छेद123(2) में यह प्रावधान है कि अध्यादेश को दोनों सदनों की फिर से बैठक होने के छह सप्ताह से अनधिक के अंदर कानून से प्रतिस्थापित करना होगा। अनुच्छेद85 में यह भी प्रावधान है कि किसी सत्र की आखिरी बैठक तथा अगले सत्र की पहली बैठक के बीच छह माह की अवधि न हो।
संस्थानों के विशिष्ट अध्यक्षगण, संकाय सदस्यगण तथा प्यारे विद्यार्थियो,
15. भारत की विविधता तथा इसकी समस्याओं का परिमाण यह अपेक्षा करता है कि संसद जन नीतियों पर एकमत तैयार करने का अधिक कारगर मंच तथा हमारे लोकतांत्रिक विचारों का वाहक बने। संसद में कार्यवाहियां सहयोग,सौहार्द तथा उद्देश्यपूर्ण भावना के साथ संचालित होनी चाहिए। बहसों की विषयवस्तु तथा स्तर उच्च कोटि का होनी चाहिए। सदन में अनुशासन तथा मर्यादा बनाए रखने तथा शिष्टाचार और शालीनता का पालन करना जरूरी है।
16. संसद को कानून निर्माण तथा नीति नर्माण करने के अपने दायित्व को जन आंदोलनों तथा सड़क पर विरोधों के आगे समर्पण नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि यह सदैव हमारी समस्याओं का सुविचारित समाधान न हो। जनता का विश्वास और भरोसा बनाए रखने के लिए संसद को ऐसी नीतियों के निर्माण के लिए कानून बनाने चाहिए जो जनता की चिंताओं और आकांक्षाओं का समाधान करें।
17. शिक्षाविद, अनुसंधानकर्ता, अभिमत निर्माता तथा भावी नेताओं के तौर पर, नीति निर्माण और इसके कार्यान्वयन की गुणवत्ता सुधार में योगदान करने में आपकी एक अहम भूमिका है। आपमें से बहुत से लोग राष्ट्र की सेवा के लिए सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने से पहले सोच समझ कर निर्णय करें क्योंकि यह किसी भी हालत में अल्पकालिक विकल्प नहीं है। परंतु एक बार जब आप निर्णय कर लें तो पूरा योगदान दें।
18. मैं, अंत में एक बार पुन: अत्यंत सुखमय और संतोषप्रद भावी वर्ष के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। यह वर्ष महान अवसरों और आपके सभी प्रयासों में सफलताओं का वर्ष हो।
धन्यवाद,
जयहिन्द!